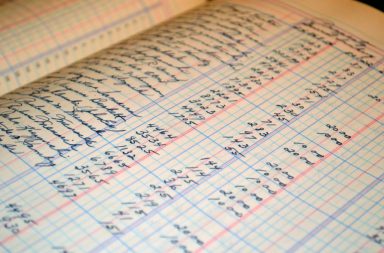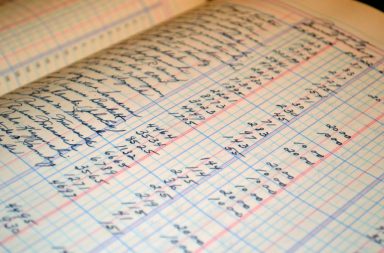डाक्टर मुकुंद नवरे
सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था मे अन्न की “संस्कृति” होती है और अन्न से संस्कृति का निर्माण भी होता है। अक्सर कहा जाता है कि जैसा हम खाते है हमारी सोच भी वैसी ही बनती जाती है। इसके बहुत से प्रमाण हैं । पिछले पचास वर्षों मे देखे कुछ उदाहरण मुझे जो याद आते है वह यह बात साबित करते है। वैसे कुछ अपवाद भी हो सकते है।
इज़राइली किबुत्झ मिशमार हॅशॅरॉन
पहला उदाहरण याद आता है इज़राइल के उस किबुत्झ का जहाँ मै सन १९७८ में पैतीस दिन रहा।उसका नाम था मिशमार हॅशॅरॉन जहां एक सौ पचास परिवार रहते थे और कुल जनसंख्या थी करीब चार सौ पचास। उनमें मेरे जैसे बाहर से आये स्वयंसेवक जोड ले तो आबादी लगभग छह सौ थी।मुद्दे की बात है कि हम सबका नाश्ता और दो वक़्त का खाना किबुत्झ के रसोई घर मे बनता था और उस रसोई घर में काम करने वाले सात आठ लोगों को छोड़ कर बाकी हम सब खेतों मे या बेकरी में या नर्सरी आदि जगहों में काम करने जाते थे।
लेकिन भोजन के वक्त सब लोग एकत्रित होकर बहुत बडे डायनिग हाल मे मज़े से खाना खाते थे। वहॉं व्हेज, नॉन व्हेज तथा डायाबेटिक नाम से तीन प्रकार के भोजन उपलब्ध हुआ करते थे। किबुत्झ का बोधवाक्य था ‘ एक के लिए सभी और सभी के लिये प्रत्येक ‘।

डाक्टर नवरे का इज़राइल प्रवास पर लिखा ब्लाग इस लिंक पर उपलब्ध है
वहाँ रहते मुझे लगा कि यदि सभी लोग साथ मे खाना खाते है तो उन मे संघ भावना का निर्माण हो ही जाता है। गौरतलब है कि उन दिनों मैने वहाँ जो सरकारी किताब देखी उसमे किबुत्झ का वर्गीकरण सहकारिता के अंतर्गत किया गया था।
इंडियन डेटोनेटर्स, हैदराबाद
दूसरा उदाहरण याद आता है हैदराबाद स्थित एक कंपनी का जो आइ डी एल केमिकल्स नाम से मशहूर थी। यह कंपनी डिटोनेटर्स याने विस्फोटक बनाती थी और उसने ग्राम-विकास (रूरल डेव्हलेपमेंट) के हेतु एक न्यास (ट्रस्ट) भी चला रखा था। था। इस संस्था का चयन एक बुल मदर फार्म स्थापित करने के लिये ऑपरेशन फ्लड परियोजना मे हुआ था।मेरा उस संस्था से संबंध इसलिये हुआ क्योंकि उस बुल मदर फार्म के लिए जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई गयी थी उसमे मैं इंडियन डेयरी कार्पोरेशन का प्रतिनिधि था।
मुझे याद आती है उस कमेटी की पहली मीटिंग जिस दिन मैं उस संस्था के उच्च अधिकारियों से पहली बार मिला। कमेटी के अध्यक्ष थे डाक्टर चटर्जी जो कंपनी के रिसर्च डायरेक्टर थे। बाकी सदस्यों मे एक डाक्टर सूर्य प्रकाश राव थे जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे। डाक्टर राव आंध्र प्रदेश के मिल्क कमिश्नर रह चुके थे। एक और सदस्य थे डाक्टर विठ्ठल राजन जो कंपनी के ग्राम-विकास न्यास के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे।
डाक्टर मुकुंद नवरे
डाक्टर मुकुंद नवरे वृक्षमंदिर के नियमित योगदानकर्ता हैं।
डॉ. मुकुंद नवरे ने डेयरी के क्षेत्र में चालीस से अधिक वर्षों तक काम किया है। वह डेयरी क्षेत्र की कई प्रमुख संस्थाओं जैसे BAIF/NDDB/मदर डेयरी दिल्ली/महानंद/जलगांव मिल्क यूनियन और डायनामिक्स से जुड़े रहे हैं। इस प्रकार वे गैर-लाभकारी, सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्रों के संगठनों की कार्य संस्कृति से परिचित रहे हैं। इन चालीस वर्षों में से, वे ऑपरेशन फ्लड परियोजनाओं से 25 वर्षों से अधिक समय तक जुड़े रहे हैं।
मुकुंद नवरे ने अपने पेशेवर जीवन के दौरान शौक़िया तौर पर साहित्यिक और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने के अवसरों की तलाश की। अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों के अलावा, उन्हें मिल्क फेडरेशन/यूनियन के लिए एक्सटेंशन बुलेटिन तैयार करने और इंडियन डेयरी एसोसिएशन (साउथ जोन) के लिए न्यूज़ बुलेटिनों का संपादन करने में भी आनंद आया। इस दौरान उन्होंने ‘डेयरी इंडिया ईयरबुक’ के निर्माण में श्री पीआर गुप्ता और शरद गुप्ता की भी मदद की और बाद में इसके संपादकीय सलाहकार समिति में काम किया और इस ईयरबुक के कई संस्करणों में कुछ लेख लिखे। डॉ. जे.वी. पारेख और उन्होंने मिलकर ‘डेयरी उत्पादों की तकनीक’ नामक पुस्तक लिखी है ।वह मुंबई से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक ‘डेयरी टाइम्स’ की सलाहकार समिति में भी हैं।
मुकुंद नवरे ने 2006 से मराठी में लघु कथाएँ लिखना शुरू किया। शुरुआत में ही उनकी कुछ रचनात्मक रचनाओं को पुरस्कार मिले। 2009 में उनकी 11 लघु कथाओं का संग्रह ‘अकल्पित कथा’ शीर्षक से विजय प्रकाशन, नागपुर से प्रकाशित हुआ। अब तक वह 55 से ज़्यादा लघु कथाएँ लिख चुके हैं, जो मराठी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, खास तौर पर उनके दीपावली संस्करणों में। 2009 में मुकुंद नवरे ने ‘दुग्धानुभव’ (अप्रकाशित) शीर्षक से डेयरी क्षेत्र में अपने अनुभवों को मराठी में लिखा। उन्होंने ‘मैत्री अनुदिनी’ के ऑनलाइन प्रकाशन में मराठी में कई लेख लिखे हैं।
इन सबके साथ वह मीटिंग तीन घंटे चली और उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने भोजन समय की घोषणा की।
“ अगर आपको आपत्ति न हो तो हम कंपनी की कैंटीन में जाकर भोजन कर सकते है।” डाक्टर चटर्जी ने मेरी ओर देखकर कहा।
“ इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है ! “ मैने जवाब दिया और हम सब कैंटीन की ओर चल पड़े।
जब वहाँ पहुँचे तब मैंने कैंटीन का हॉल इतना बड़ा देखा जहां आराम से लगभग एक हजार लोग एक साथ भोजन कर रहे थे। “ हमारी कंपनी में वर्कर्स आदि मिलकर तीन हजार लोग है और हम सब यही भोजन करते है।” डाक्टर चटर्जी ने जानकारी दी।
मैंने सभी ओर देखा और पाया कि हर तरह से एक आदर्श व्यवस्था थी। एक ओर अनगिनत टेबल थे जहां बैठे लोग आनंद से खाना खा रहे थे। दूसरी ओर एक कतार थी जिसमें हाथ मे थाली लिये लोग खडे थे और शांति से आगे बढते जा रहे थे जहाँ काउंटर से अलग अलग व्यंजन परोसे जा रहे थे।
हम सभी कमेटी सदस्यों ने एक टेबल पर रखी जो थालियाँ थी उनमें से एक एक थाली उठायी और हम भी कतार मे लग गये। अब एक ही मिनिट हुआ होगा कि डाक्टर चटर्जी बोल उठे,“ वहाँ आगे एम् डी साहब भी है, चलो उनसे मिल लेते है ।”
वह मुझे साथ लेकर कुछ कदम आगे चलते गये। जैसे हम पहुँचे, उन्होंने मेरी एम डी साहब से पहचान करा दी। उनसे दो शब्द बोलकर हम पीछे आकर कतार मे लग गये। डाक्टर चटर्जी ने कहा कि वह महोदय वरदराजन कंपनी के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है, और विदेश आते जाते रहते (ग्लोब ट्रॉटर) है।
उनको यहाँ मिल पाना हर समय संभव नही होता।
मुझे आश्चर्य लगा कि इस दर्जे का व्यक्ति अपनी थाली खुद उठाकर अपनी कंपनी की कैंटीन में वर्कर्स के साथ कतार में कैसे खडा रह सकता है ? स्वाभाविक तो यही है कि वह अपनी केबिन मे किसी अच्छे होटल से मंगाया खाना खाए या तो उसके घर से टिफिन कैरियर मे आये और चपरासी खाना प्लेट मे भरकर साहब के लिये अलग टेबल पर लगा दे।
देखो, यह जो अन्न है, इसकी व्यवस्था ऊपर वाला करता है। हम तो एक माध्यम है ठीक से जान लो। यहाँ जो काम कर रहे है उनका भोजन भी वह उनका हक़ है। हम कोई एहसान नही करते
हनुमंत राव
मेरे पूछने पर डाक्टर चटर्जी ने बताया कि कंपनी का हर एक व्यक्ति कैंटीन मे खाना खाए यह निर्देश खुद वरदराजन जी का दिया हुआ है और उससे न तो वे अलग है न हम कोई। वरदराजन जी कहना है कि जब सभी कर्मचारियों के साथ हम यहाँ भोजन करेंगे तो भोजन की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। जो थालियाँ हम टेबल से उठायेंगे वह ठीक से धुली हुई हैं या नहीं यह भी हमें दिखाई देगा।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कतार में आकर खाना लेते है तो कॉन्ट्रैक्टर ने सबके लिए जो खाना बनाया है वहीं हमें भी मिलेगा।हमारे लिये अलग भोजन वह नहीं बनायेगा।
उसके बाद जब हम हाथ मे भरी थाली लेकर गये तब सी एम डी वरदराजन जी जहां बैठे थे उसी टेबलपर हम जा बैठे। उन्होंने बुल मदर फार्म के बारेमे पूछताछ की तब पता चला कि डेयरी फार्म के बारे में सब रिपोर्ट उन्हे मिलती रहती है और वे पढते भी है । उसी दिन मुझे पता चला कि वह एक खास कंपनी है जिसके सभी कर्मचारी सुरक्षा हेतु बाहर रहते है। क्योंकि उनका कोई कैम्पस नही है इसलिए मेलजोल बना कर रखने के लिए सामुदायिक भोजन जरूर बहुत काम आता है । लेकिन उसके अलावा कुछ और भी नया मुझे सीखने को मिला।
मैनेजिंग डायरेक्टर हनुमंत राव की डेयरी
अब याद आता है एक डेयरी कंपनी का उदाहरण जहां मै सलाह देने के हेतु से हर महीने जाता था। उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हनुमंत राव थे। उस डेयरी का दैनिक कारोबार करीब तीस हज़ार लीटर का था और उसमे बढोतरी होने की संभावना बहुत दूर की थी। इसी कारण से उनके जितने सारे खर्चे थे उन पर नियंत्रण रखना जरूरी था। इस पर सोच विचार करने के बाद कंपनी के जितने सारे विभाग थे उन सभी को आदेश दिया गया कि वे अपने अपने खर्चे कम करें तथा इस बारे मे उनके कोई सुझाव हों तो अवश्य दें। इसमे एक कार्मिक विभाग था जो कंपनी के वर्कर्स कैंटीन का हिसाब रखता था। एक दिन ऐसा आया कि जब कार्मिक अधिकारी एक प्रस्ताव ले आया जिसमें कैंटीन का खर्च कम करने की बात थी।
“ सर, मेरा सुझाव है कि हम जो खाना देते है…” वह बोल उठा।
जैसे उसने शुरुआत की तो हनुमंत राव ने उसे एकदम टोक दिया।
“ यहाँ कोई किसी को खाना नही देता, न तुम न मैं।गलतफहमी में न रहो।” हनुमंत राव बोले।
यह सुनकर कार्मिक अधिकारी चकित हुआ।
“ देखो, यह जो अन्न है, इसकी व्यवस्था ऊपर वाला करता है। हम तो एक माध्यम है ठीक से जान लो। यहाँ जो काम कर रहे है उनका भोजन भी वह उनका हक़ है। हम कोई एहसान नही करते।” हनुमंत राव बोले।
उसके बाद कार्मिक अधिकारी ने जो प्रस्ताव किया वह भी उन्होंने नकारा क्योंकि उसमे हर एक वर्कर की थाली मे परोसे जाने वाली रोटियाँ, चावल पर कुछ नियंत्रण लाने की बात थी।हनुमंत राव ने उनसे कहा कि और जगह खर्चे कम करें लेकिन वर्कर को पेटभर खाना हर हालत मे मिलना चाहिए।
आगे चलकर हमने कई जगहोंपर होने वाले खर्चे कम कर दिये लेकिन वर्कर्स के भोजन पर होने वाले खर्च पर कोई ऑंच नही आने दी। इस अनुभव से मुझे भी एक नई सीख मिली।
घर मे कार्यालय और भोजनालय
अब उदाहरण है एक छोटी सी फर्म का जहां मेरे रिश्ते में आनेवाले एक आर्किटेक्ट के साथ उनके पाँच सहकर्मी काम करते थे। यह फर्म उनके घर से ही चलती थी क्योंकि घर बहुत बड़ा था और उसे कार्यालय के रूप मे परिवर्तित करना आसान था।दूसरी बात यह थी कि उनकी पत्नी दूसरी जगह काम करती थी इसलिए हमेशा घर पर नही होती थी बल्कि कभी-कभी आया करती थी। अब इस तरह रहते हुए आर्किटेक्ट महोदय ने सोचा कि उनके सभी सहकर्मियों का दोपहर का खाना एक साथ घर के रसोईघर मे बन सकता है क्योंकि सभी चीजें वहाँ मौजूद होती थीं। जो कुछ खाद्य सामग्री हर महीने ख़रीदी जाती है उसमे बढोतरी होगी लेकिन सबका खाना भी तो बनेगा। जैसे यह विचार उन के मन मे आया उन्होंने अपने सहकर्मियों के साथ चर्चा की और अपनी कल्पना को साकार भी कर दिया।
जब मुझे इस बात का पता चला तब लगा कि इस उपक्रम को जाकर देख लेना चाहिए।
“मै तो मानता हूँ कि यही मेरा कुटुंब है। हम एक साथ काम करते हैं वैसे ही एक वक्त का भोजन भी एक साथ करते है। और जो कुछ खर्चा होता है वह भी मेरे लिये नगण्य है।अब मुझे कोई चिंता भी नहीं है, कल अगर अकेले में मुझे कुछ हो जाता है तो यही लोग है जो मुझे अस्पताल भी ले जाएँगे”
मैंने आर्किटेक्ट महोदय से इच्छा जताई तो उनके आमंत्रण पर उनके यहाँ जाकर मैंने दो दिन बिताए। मैं जानता था कि उनकी दो बेटियाँ शादीशुदा है, एक तो विदेश में रहती है। पत्नी भी दूर थी लेकिन अगले सप्ताह आनेवाली थी। पहले दिन हम सुबह उठकर टहलने के लिए निकल पड़े तब उन्होने काफ़ी थैलियाँ साथ में ले ली। उनकी गाडी से हम दूर तक गये और गाडी किसी जगह पार्क करके पैदल चलते रहे। वहाँ से लौटते समय एक रेस्टोरेंट में जाकर हमने नाश्ता भी कर लिया। अब इसके बाद वे मुझे सब्ज़ी मंडी ले गए जहां उन्होंने काफी सारी सब्ज़ियाँ खरीद डाली।उन्होंने बताया कि इतनी सारी सब्ज़ियों से एक सप्ताह तो निकल जाता है।
हम घर लौटे तब तक घर साफ करनेवाली बाई आ चुकी थी। उसने शीघ्र गति से अपना काम किया और उस दिन उपयोग में आने वाली सब्ज़ियों को छोडकर बाकी फ्रिज में डाल दी। मुझे पता चला कि रसोई बनाने का काम भी वहीं करती है। लेकिन कौन से दिन क्या बनेगा यह दूसरे सहकर्मी निश्चित करते है। बाजार से चीजें खरीद कर लाना आर्किटेक्ट महोदय खुद करते है यह तो मैंने देखा था। बस, काम का बँटवारा इतना ही था। लेकिन कुछ नियम थे जिससे कि कोई चीज बेकार न जाए याने कि, नो वेस्टेज।यहाँ तक कि हर एक सहकर्मी को बताना पडता था कि उसे कितनी रोटियाँ चाहिए।
उसके बाद एक एक करके बाकी सहकर्मी काम पर आये और कार्यालय शुरू हुआ। तब तक आर्किटेक्ट महोदय भी नहा धोकर आ गये थे और अपनी कुर्सी पर विराजमान थे।उस दिन मैंने उनके कार्यालय का काम चलते देखा। दोपहर एक बजे जब सभी सहकर्मी भोजन करने बैठे तब उनके साथ मैंने भी भोजन किया।
सहकर्मियों में तीन महिलाएँ थी उन्होंने भी खाना लगाने में मदद की। खाना घरेलू था, ताज़ा था और सबकी पसंद का था। खाते समय इधर उधर की बातें हो रही थी। यह देखकर मुझे लगा कि आर्किटेक्ट महोदय का सबके लिए खाना वहीं पर बनाने का निर्णय ठीक था । शायद वही कारण होगा जिससे उस कार्यालय में टीम स्पिरिट बन चुकी था।
बाद मे जब मेरी चर्चा हुई तब आर्किटेक्ट महोदय बोले, “ देखो, मै तो मानता हूँ कि यही मेरा कुटुंब है। हम एक साथ काम करते हैं वैसे ही एक वक्त का भोजन भी एक साथ करते है। और जो कुछ खर्चा होता है वह भी मेरे लिये नगण्य है।अब मुझे कोई चिंता भी नहीं है, कल अगर अकेले में मुझे कुछ हो जाता है तो यही लोग है जो मुझे अस्पताल भी ले जाएँगे।” उनकी सोच मुझे बहुत भा गई।
रेस्टोरेन्ट के कर्मचारियों का भोजन
अब जो उदाहरण है वह तो ऐसी कंपनी का है जो खुद खानपान की इंडस्ट्रीमे कदम रख चुकी थी। इसके जो प्रवर्तक थे उनकी डेयरी कंपनी को मै सलाह देता था इसलिये वे फूड कंपनी के बारे में मुझसे मशवरा करते थे। उन्होंने सॉफ्टी आइसक्रीम के साथ फास्ट फूड के केंद्र भी खोले थे। बाद में उन्होंने सोचा कि वे रेस्टोरेन्ट भी खोल सकते हैं। परिणाम स्वरूप उनका पहला रेस्टोरेन्ट उडिपीके पास एक जगह खोला गया। यहाँ जो मेनू बनाया गया उसमें दक्षिण भारतीय, पंजाबी तथा कॉन्टिनेन्टल ऐसी तीन तरह का खाना बनना शुरू हुआ।
कुछ ही दिनों में रेस्टोरेन्ट में अलग विभाग तथा दो शिफ्टमे काम करनेवाले कर्मचारियों संख्या अस्सी नब्बे तक पहुँच गई।
“वह कांदे (प्याज) की आमटी अच्छी बनी थी और मैंने अपने लिये रखीं थी।मैं सिर्फ चावल के बारे में बोलकर गया था। तुम कुछ ध्यान नही देती, सिर्फ टीवी देखती रहती हो”
अब मुद्दे की बात आती है कि रेस्टोरेन्ट के इतने सारे कर्मचारियों के खाने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिये। जब इस पर विचार हुआ तब मुझे पता चला कि हर जगह रेस्टॉरेंट स्टाफ़ के लिए अलग खाना सुबह शाम बनाया जाता है और वह एक थंब रूल है जिसकी अलग व्यवस्था होती है। कारण यह है कि जो ख़ाना ग्राहकों के लिए तैयार किया जाता है वह किसी दिन या दो चार दिन के लिए ठीक है। लेकिन हर रोज़ उसे खाना सेहतमंद नही होता यह फूड इंडस्ट्री जानती है। इसलिये स्टाफ की सेहत का खयाल करना पड़ता है।
इससे विपरीत एक उदाहरण मैंने वही पर एक कॉल सेन्टर में देखा।वहाँ हम दो सौ लोगोंका खाना रात में सप्लाई करते थे। मैनेजमेंट चाहती थी की खाना बिल्कुल होटल की तरह हो जिससे रात भर काम करने वाले युवक युवतियों के लिए वह एक आकर्षण बना रहे और वे काम न छोड़ें। ऐसा हुआ भी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके बहुत से कर्मचारियों को एसिडिटी होने लगी। बादमे वे कहने लगे कि खानें में तेल और तीखा हम कम करे। मैनेजमेंट के लिए यह एक मेसेज था।
उदार और संकुचित सोच
इन सभी उदाहरणों से लगता है कि भोजन का विचार जब सामुदायिक स्तर पर होता है तो सोच भी उदार हो जाती है। इससे विपरीत जब भोजन कुछ एक लोगों तक सीमित होता है तो शायद सोच भी संकुचित हो जाती है। इसका एक उदाहरण मुझे याद आता है।
यह करीब बीस साल पहले की बात है जब मै एक ऑन्टी को मिलने उनके घर गया था।उनकी उम्र पचासी सालकी हो चुकी थी और वह अपने पुत्र के घर वे शांति से रह रही थी। मैं जब मिलने गया तब सुबह के ग्यारह बजे थे। उनका बेटा और बहू दोनों कही बाहर गये थे और वह घर मे अकेले थी और कोई टेलीविजन चैनल देख रही थी।वैसे भी अब घर का कोई काम करने की शक्ति उनमें नहीं थी तो बस, टेलीविजन देखकर वह अपना मनोरंजन करती होगी।ऑन्टी ने मुझसे बातें तो की लेकिन वह टेलिविज़न भी देखती रही।
करीब बीस मिनिट बाद उसका बेटा घर लौटा तो हमारी कुछ बातें हुई।फिर वह अंदर रसोईघरमे गया और तड़ाक से वापस लौटा।एकाएक उसने ऊँची आवाज़ में अपनी माँ से बात करना शुरू किया।
“ मैंने तुमसे जाते समय कहा था,भिखारी आयेगा तो उसे कल रात के चावल देने है।” वह बोला।
“ मैंने दे दिये।” ऑन्टी बोली।
“ लेकिन तुमने कांदे की आमटी भी दे दी!” बेटा बोला।जैसे कौई आपत्ति गिर पड़ी हो।(आमटी याने तडका दी हुई खट्टी दाल)
“ बेटे,आमटी दी तो क्या हुआ ? ” ऑन्टी बोली।
“ वह कांदे (प्याज) की आमटी अच्छी बनी थी और मैंने अपने लिये रखीं थी।मैं सिर्फ चावल के बारे में बोलकर गया था। तुम कुछ ध्यान नही देती, सिर्फ टीवी देखती रहती हो।” बेटा बोला।
“ लेकिन बगैर दाल वह सूखा चावल कैसे खायेगा मैंने सोचा।” ऑन्टी बोली।
“ उसकी फ़िक्र तुम्हें क्यों, उसे दाल तो और घरों से भी मिल सकती है।” बेटे ने ग़ुस्से में कहा।
बाद में वह मुझसे बातें करने लगा। लेकिन जो कुछ हुआ था उसकी नाराज़गी चेहरे से छिप नहीं रही थी। मैं सोचता रहा कि पैंसठ सालकी उम्र होकर भी मन की सोच इतनी संकीर्ण कैसे हो सकती है।